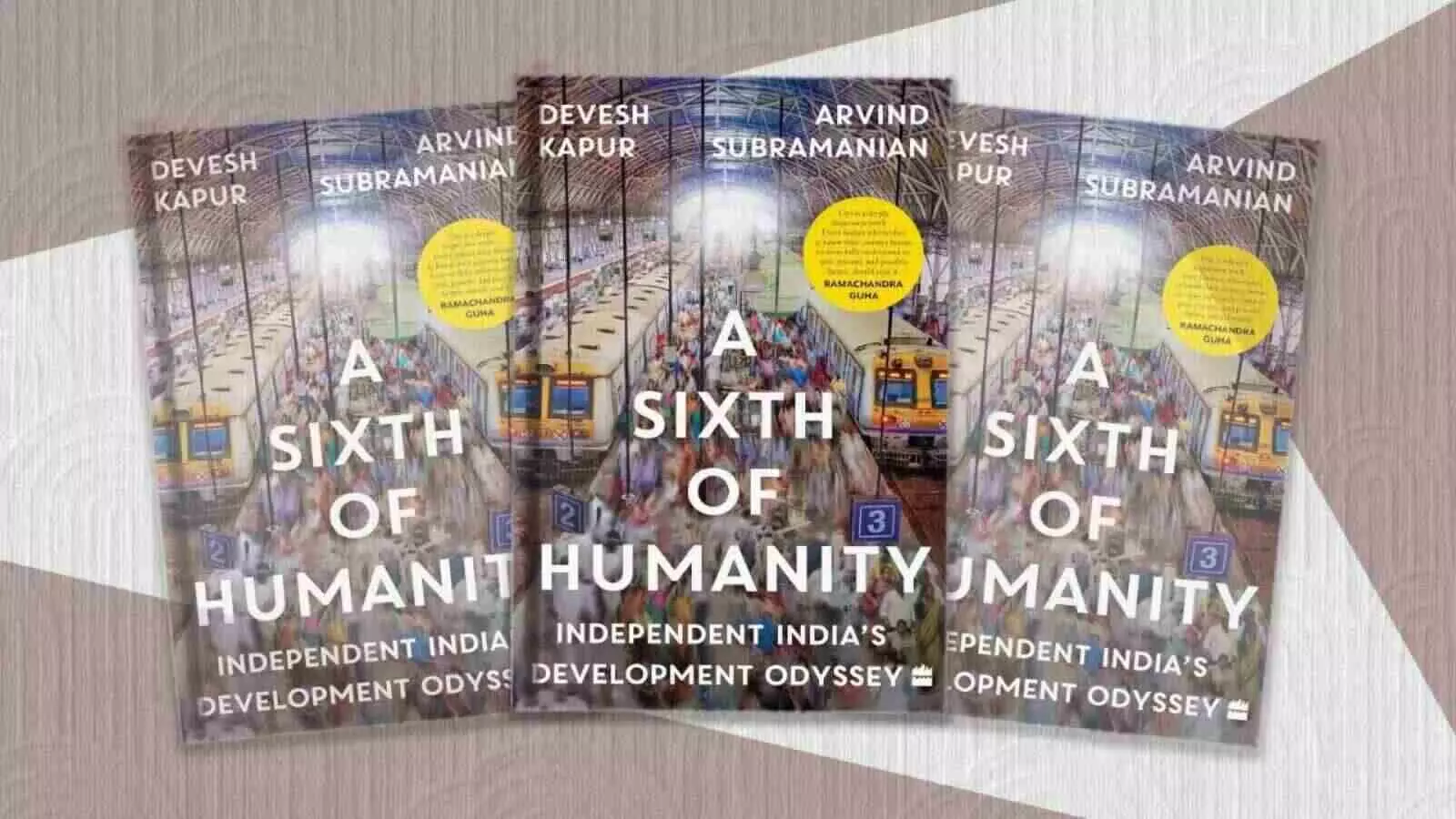
भारत के भाषाई संघवाद ने राष्ट्रीय भाषा को लेकर संघर्ष को कैसे आकार दिया
'ए सिक्स्थ ऑफ़ ह्यूमैनिटी' के इस हिस्से में, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम बताते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल देश बनाने की चुनौतियाँ अक्सर केंद्र की खुद को काबू में रखने की हिम्मत की कमी की वजह से सामने आती हैं।

A sixth of humanity : देश बनाने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है बातचीत का एक आम ज़रिया, एक 'राष्ट्रीय भाषा’। भारत की भाषाई विविधता, क्षेत्रीय भाषाओं का उसका समृद्ध इतिहास, जो उनकी संस्कृतियों और सब-नेशनलिज़्म की शुरुआत थीं, को देखते हुए, 1950 के दशक में यह सबसे बड़ी चुनौती थी। एक मल्टीनेशनल देश बनाने की चुनौतियाँ समय-समय पर वापस आती रहती थीं, अक्सर केंद्र सरकार की खुद को रोकने की हिम्मत की कमी के कारण। और, बदले में, यह मुद्दा भारत के फ़ेडरलिज़्म से जुड़ा था।
भारत में फ़ेडरलिज़्म कई मामलों में अलग था। पहला, यह एक ‘यूनियन’ था। एक ‘एक साथ रखने वाला’ फ़ेडरलिज़्म और US के उलट ‘राज्यों का फ़ेडरेशन’ नहीं था, जिसे ‘एक साथ आने वाला’ फ़ेडरलिज़्म बताया गया है। संविधान सभा साफ़ थी कि भारत ‘एक यूनियन है क्योंकि यह कभी न टूटने वाला है... देश एक ही है’। ‘इंटीग्रल होल’ को कुछ बेसिक मामलों में एक जैसा होने से सपोर्ट मिला, जिसमें कानून, एक ज्यूडिशियरी और एक ऑल-इंडिया सिविल सर्विस शामिल थे।
हिंदी और तमिल के बीच टकराव
हालांकि संविधान ने पार्लियामेंट को नए राज्य बनाने का अधिकार देकर यूनियन को बहुत ज़्यादा ताकत दी, लेकिन इससे फेडरेशन को सब-नेशनल उम्मीदों पर खरा उतरने और जवाब देने का भी मौका मिला, जो भारत के अंदरूनी पॉलिटिकल भूगोल में समय-समय पर होने वाले बदलावों से साफ है। शुरुआती बदलाव 1947, 1950, 1952 में रियासतों के मिलने के जवाब में हुए थे। 1953 में आंध्र राज्य (मद्रास से अलग) से शुरू होकर, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 के तहत इंडियन यूनियन की अट्ठाईस यूनिट्स (पार्ट्स A, B और C राज्य और पार्ट D इलाका-अंडमान और निकोबार आइलैंड्स) को मिलाकर बीस यूनिट्स चौदह राज्य और छह यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। 63 साल बाद, 2019 में जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद, भारत में दोगुने राज्य (अट्ठाईस) और आठ केंद्र शासित प्रदेश थे।
बातचीत का एक आम ज़रिया एक लिंगुआ फ़्रैंका हमेशा से राष्ट्रवाद और राष्ट्र-निर्माण के सबसे असरदार तरीकों में से एक रहा है। अंग्रेज़ी अमीर लोगों की भाषा थी (1951 की जनगणना में मुश्किल से 1 प्रतिशत आबादी अंग्रेज़ी बोलती थी), जो ज़्यादातर ऊँची जातियों के थे। इसके अलावा, इतने समृद्ध भाषाई परंपराओं वाले देश के लिए, गुलाम बनाने वालों की भाषा को सरकारी भाषा बनाने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। जैसा कि महान केन्याई लेखक न्गुगी वा थिओंगो ने बाद में कहा, ‘कॉलोनाइज़्ड लोगों का कॉलोनाइज़र की भाषा पर दावा करने की कोशिश करना गुलामी की सफलता की निशानी है।’
लोगों के बीच बातचीत के एक कॉमन तरीके की ज़रूरत को देखते हुए, हिंदी को आम भाषा बनाने का काफ़ी दबाव था, जो (और उससे मिलती-जुलती भाषाओं के साथ) 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 44 प्रतिशत आबादी की मातृभाषा थी। लेकिन एक बहुभाषी देश में, जहाँ दूसरी भाषाओं का समृद्ध इतिहास रहा है, एक ही भाषा को बहुत ज़्यादा ज़ोर देना, उसे टूटने का एक संभावित ज़रिया भी बना सकता है (जैसा कि पाकिस्तान में उर्दू के साथ हुआ था), जहाँ क्षेत्रीय राष्ट्रवाद भाषाई पहचान में निहित है।
हिंदी को आम भाषा के तौर पर बढ़ावा देने का, हैरानी की बात नहीं है, दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ बंगाल ने भी कड़ा विरोध किया। इसके सबसे जोशीले समर्थकों ने बड़ी आम भाषा, हिंदुस्तानी को अपनाने से साफ़ मना करके, जोश में फ़ारसी से वोकैबुलरी हटाकर, देवनागरी लिपि इस्तेमाल करने पर ज़ोर देकर और हिंदी न बोलने वालों के लिए आसान रोमन लिपि पर विचार करने से मना करके अपने ही मकसद को कमज़ोर कर दिया, जिससे पूरे देश में ज़्यादा बराबरी का मौका मिल सकता था।
जबकि स्विट्जरलैंड और यूगोस्लाविया जैसे दूसरे देश भी कई भाषाएँ बोलने वाले थे, भारत इस मायने में अलग था कि अलग-अलग भाषाओं की अपनी स्क्रिप्ट भी थीं, और साथ ही इसका साहित्यिक इतिहास भी बहुत समृद्ध था। 1950 के दशक में मद्रास (तमिल बनाम तेलुगु) और असम में भाषा से जुड़े झगड़े शुरू हो गए, जहाँ यह उस राज्य की बड़ी बंगाली आबादी द्वारा बंगाली भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ था।
हालांकि, सबसे गंभीर झगड़ा हिंदी और तमिल के बीच था। यह मद्रास (बाद में तमिलनाडु) में शुरू हुआ, जहाँ द्रविड़ कज़गम (DK, और बाद में इसकी शाखा, DMK) के नेतृत्व वाले द्रविड़ आंदोलन ने अपनी पहचान दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के खिलाफ से हिंदी के खिलाफ और फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ बनाई, बड़ी चालाकी से पहले को बाद के दो से जोड़ा। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए 'लिंग्विज़्म' की ताकत का नेतृत्व कॉलेज के छात्रों ने किया, जिन्हें महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय अभिजात वर्ग ने बढ़ावा दिया।
आज़ादी की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी
मूल समस्या वही थी जिसका ज़िक्र चैप्टर II में किया गया है: नौकरियों में उसी हिसाब से बढ़ोतरी के बिना हायर एजुकेशन का तेज़ी से विस्तार। भाषा पर ज़ोर एंट्री में रुकावटें बढ़ाने और कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए उतना ही था जितना कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की जान खोने के डर से। 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से यह समस्या कुछ हद तक ही हल हुई। 1961 की जनगणना में पाया गया कि भारत में किसी भी राज्य/UT में बारह से कम मातृभाषाएँ नहीं थीं (मातृभाषाओं की संख्या 12-410 के बीच थी)। इस प्रकार, मूल रूप से सभी राज्य बहुभाषी संस्थाएँ थीं, भले ही राज्यों के गठन में विभिन्नता हो। एकल या द्विभाषीय मानदंड पर सीमाएं।
लेकिन अगर साउथ में हिंदी थोपने के खिलाफ़ आवाज़ें थीं, जिसमें ऑफिशियल भाषा के तौर पर इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई थी, तो नॉर्थ के राज्यों में भी इंग्लिश के खिलाफ़ उतने ही ज़ोरदार विरोध थे, एक ऐसी भाषा जिससे वहां की पिछड़ी जातियां नाराज़ थीं क्योंकि यह ऊंची जातियों की दबदबे वाली ताकत को और मज़बूत करती थी। इसके उलट, उन्नीसवीं सदी के आखिर में सोशल रेवोल्यूशनरी सावित्रीबाई फुले से लेकर एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद दलित इंटेलेक्चुअल चंद्रभान प्रसाद तक, इंग्लिश को दलितों की मुक्ति की भाषा के तौर पर देखा गया।
सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि इंडिया के रूलिंग एलीट की तीन मुख्य खासियतें थीं - जाति का स्टेटस, पैसा और इंग्लिश एजुकेशन। उनके शिष्य कर्पूरी ठाकुर के बिहार में मैट्रिक पास करने के लिए इंग्लिश को ज़रूरी सब्जेक्ट के तौर पर खत्म करने के बाद, हायर एजुकेशन में पिछड़ी जातियों के गांव के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन तेज़ी से बढ़ा।
लेकिन बिहार में पहुंच बढ़ाने के फायदे तेज़ी से बिगड़ते हायर एजुकेशन सिस्टम की वजह से कम हो गए। पिछड़ी जातियों को ज़हरीला प्याला नहीं मिला, बल्कि खाली प्याला मिला। भाषाओं को आगे बढ़ने के लिए डायनैमिक होना पड़ता है। उत्तर भारत में यूनिवर्सिटीज़ के खत्म होने से हिंदी की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा के स्रोत सूख गए। STEM फ़ील्ड में सबसे अच्छी टेक्स्टबुक्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिशें भी बहुत कम हुईं। हिंदी फैली, लेकिन ज़्यादातर नॉन-स्टेट ट्रांसमिशन चैनलों के ज़रिए, बॉलीवुड फ़िल्मों और म्यूज़िक से लेकर बीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में नौकरी के लिए उत्तर भारत जाने वाले दक्षिण भारत के माइग्रेंट्स तक और फिर अगली सदी में इसके उलट, साथ ही सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन्स की कोशिशों से। हालाँकि, इन ट्रेंड्स को बढ़ावा देने के बजाय, केंद्र सरकार द्वारा ज़बरदस्ती की नई सोच ने भाषाई आग को फिर से भड़काने का खतरा पैदा कर दिया।
(देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम की किताब 'अ सिक्स्थ ऑफ़ ह्यूमैनिटी: इंडिपेंडेंट इंडियाज़ डेवलपमेंट ओडिसी' से लिया गया, हार्पर कॉलिन्स इंडिया से अनुमति लेकर। लेखक 3 दिसंबर को चेन्नई के ग्रेट लेक्स कैंपस में द फेडरल के एडिटर-इन-चीफ एस. श्रीनिवासन के साथ उनकी नई आइडिया सीरीज़, 'वॉयसेज़ दैट काउंट' के हिस्से के तौर पर बातचीत करेंगे।)

