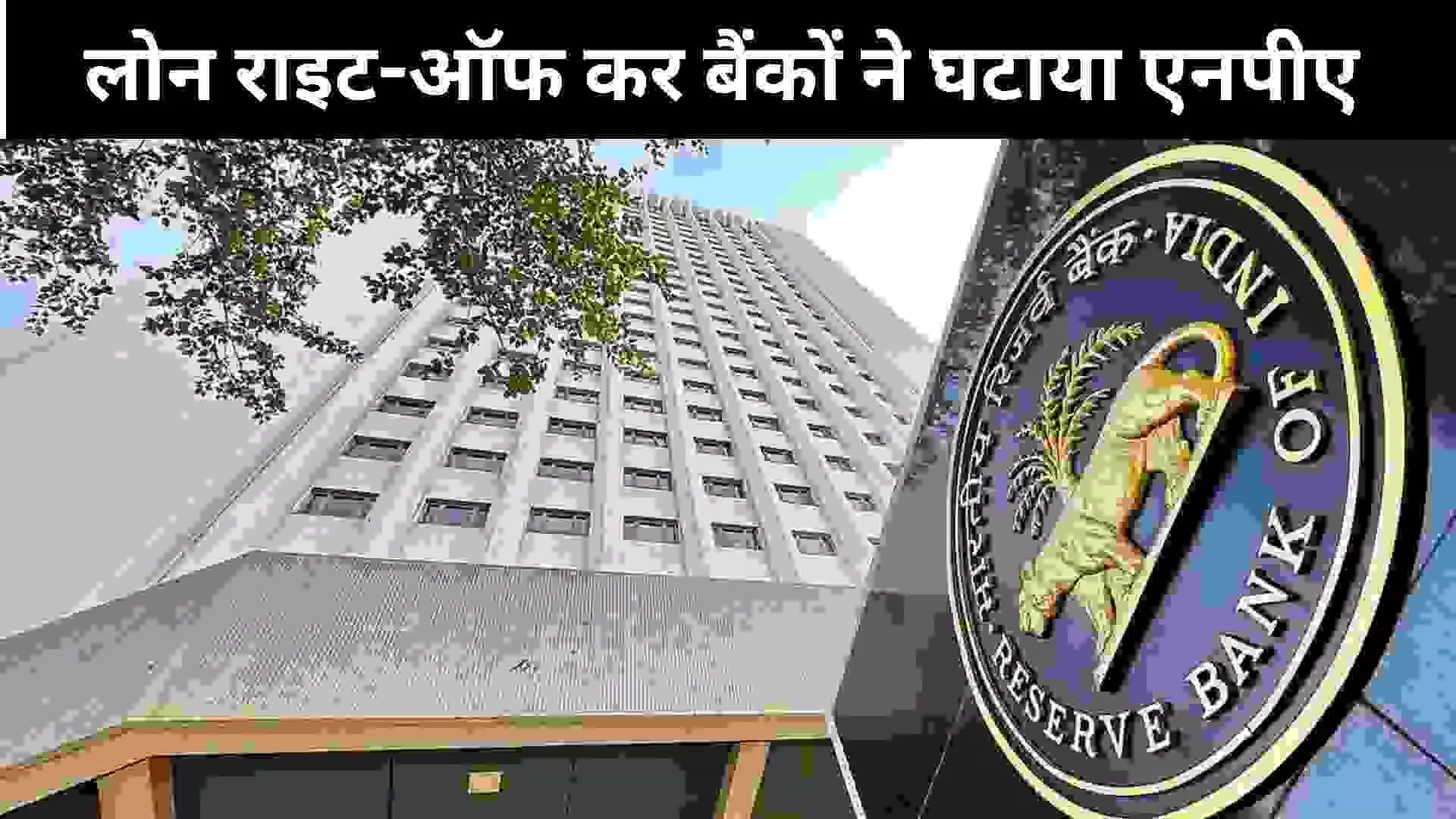
कर्ज की वसूली नहीं बल्कि 5 सालों में लोन को Write-Off कर बैंकों ने घटाया एनपीए
RBI की एक रिपोर्ट ने बैंकों के NPA में कमी के कारणों का खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक एनपीए वाले अकाउंट्स बंद कर लोन को write off किया इसलिए बैंकों का एनपीए अब कम दिख रहा है.

हाल के वर्षों में सरकार की तरफ से, आरबीआई की ओर से बार-बार कहा गया है कि कुछ वर्ष पहले भारत का बैंकिंग सेक्टर जो एनपीए की समस्या से जूझ रहा था उसपर अब काबू पा लिया गया है. ग्रॉस एनपीए रेश्यो यानी बैंकों का ऐसा कर्ज जो डूब गया वो अब कई दशकों के सबसे निचले लेवल 2.3 फीसदी पर और नेट एनपीए 0.5 फीसदी पर आ गया है. नए एनपीए बनने की दर भी 0.7% पर स्टेबल बना हुआ है.
एनपीए के कम होने की वजह पर गौर करें तो ऐसा नहीं है कि बैंकों ने जिन्हें कर्ज दिया था उनसे कर्ज वसूली में बैंकों को बड़ी सफलता मिली है. एनपीए के घटने की बड़ी वजह है बैंकों द्वारा लोन का राइट-ऑफ किया जाना यानी कर्ज की वसूली नहीं होने पर उसे बट्टे खाते पर डाल जाना. इसी के चलते बैंकों का एनपीए अब कम दिखाई दे रहा है.
बैंकों ने राइट-ऑफ कर घटाया NPA
इसका खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक के फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में किया गया है जिसे आरबीआई ने जारी किया है. आरबीआई के मुताबिक शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के डूबे कर्ज यानी ग्रॉस एनपीए रेश्यो में राइट-ऑफ (write-off) 2024-25 में बढ़कर 31.8 फीसदी पर जा पहुंचा है जो कि 2023-24 में 29.5 फीसदी हुआ करता था. आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉस एनपीए रेश्यो में सबसे ज्यादा राइट-ऑफ प्राइवेट और विदेशी बैंकों में किया गया है. जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राइट-ऑफ में मामूली कमी आई है. आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बैंकों ने अपने एनपीए का सबसे ज़्यादा हिस्सा write-off करके ही घटाया है ना कि डूबे हुए कर्ज की वसूली करके.
10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये Write-Off
दरअसल बीते एक दशक में बैंकों के सामने एनपीए सबसे बड़ी समस्या रही है. पिछले 10 वर्षों बैंकों को 16.35 लाख करोड़ रुपये के डूबे हुए कर्ज को राइट-ऑफ करना पड़ा है. बजट सत्र के दौरान सरकार ने लोकसभा में ये डेटा पेश किया था. साल 2014-14 में 58,786 करोड़, 2015-16 में 70413 करोड़, 2016-17 1.08 लाख करोड़, 2017-18 में 1.61 लाख करोड़, 2018-19 में 2.36 लाख करोड़, 2019-20 में 2.34 लाख करोड़, 2020-21 में 2.04 लाख करोड़, 2021-22 में 1.75 लाख करोड़, 2022-23 में 2.16 लाख करोड़ और 2023-24 में 1.70 लाख करोड़ जो कर्ज डूब गया था बैंकों ने उसे राइट-ऑफ किया है.
क्या होता है एनपीए?
NPA फुल फॉर्म है Non-Performing Asset. जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन लेकर समय पर किस्तें 90 दिन या उससे ज्यादा समय तक नहीं चुकाता है, तो बैंकों को उस लोन को एनपीए घोषित करना पड़ता है. जब बैंकों के लिए उस कर्ज को वसूलना नामुमकिन हो जाता है तो बैंक उसे लोन को राइट-ऑफ कर देते हैं यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं हालांकि उस कर्ज को वसूलने की प्रक्रिया बैंकों की ओर से जारी रहती है.
एनपीए का बैंकों पर असर
एनपीए का बैंकों पर बेहद बुरा असर पड़ता है. आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए बढ़ने का असर बैंकों के बैलेंसशीट पर पड़ा था. बैंकों का नुकसान बढ़ गया था और उनके मुनाफे में भारी कमी आ गई. बैंकों के कर्ज पर ब्याज मिलना बंद हो गया उसपर से कर्ज भी डूब गया. बैंक को ऐसे लोन के लिए अलग से पैसे की प्रॉविजनिंग करना पड़ता है जिसमें अलग से पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, जिससे मुनाफा और कम हो जाता है.
एनपीए बढ़ने से बैंक के पास कम पैसा बचता है, जिससे वह नए ग्राहकों को कर्ज देने में सावधानी बरतता है या सख्ती करता है. ज्यादा एनपीए के चलते ग्राहक और निवेशक दोनों का भरोसा कमजोर होता है.
कैसे RBI ने उबारा बैंकों को संकट से
एनपीए बढ़ने के चलते जब पब्लिक सेक्टर बैंक वित्तीय संकट में आ गए तो आरबीआई ने बैंकों को PCA (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) फ्रेमवर्क में डाला जिससे बैंक को संकट से उबारा जा सके. RBI चार फैक्टर्स जिसमें Capital Adequacy Ratio, Asset Quality यानी NPA का स्तर, मुनाफा और कर्ज के स्तर को देखकर ऐसा करता है. जब भी कोई बैंक PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, तो RBI उस पर पाबंदियाँ लगाता है जिससे समय रहते बैंक की वित्तीय हालत सुधारा जा सके.

