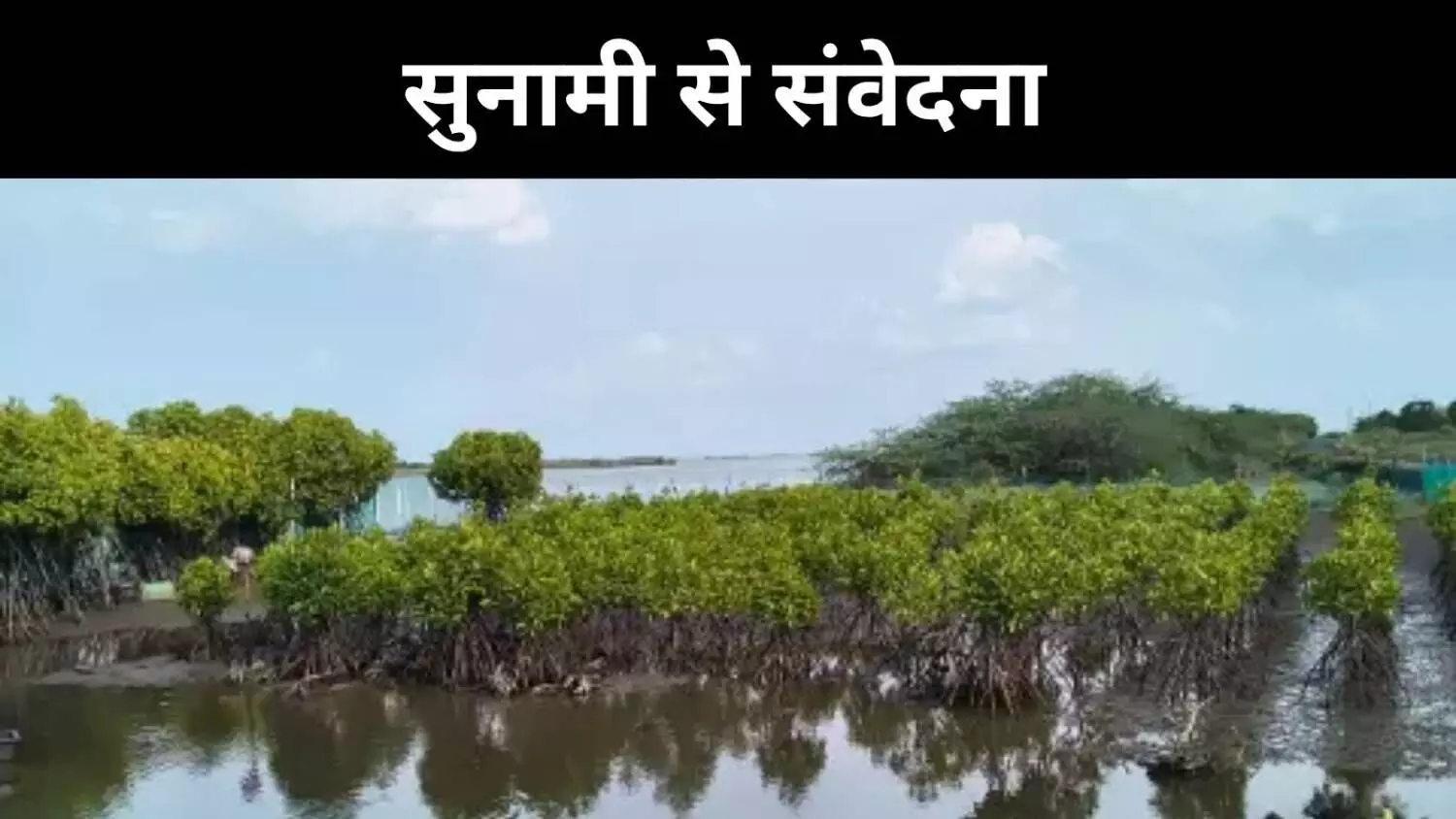
एक व्यक्ति, एक जंगल, वीरप्पन ने कैसे बदली तमिलनाडु के पिचावरम की किस्मत
तमिलनाडु के वीरप्पन ने सुनामी के बाद मैंग्रोव और क्रैब फैटनिंग से न सिर्फ पर्यावरण बचाया, बल्कि गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया।

कडलूर ज़िले के पिचावरम कस्बे में स्थित कलैग्नर नगर का एक निवासी दुरईसामी वीरप्पन बचपन से ही मैंग्रोव जंगलों से परिचित था। यह इलाका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का घर है, सुन्दरबन के बाद। मगर, अपने समकालीन लोगों की तरह वीरप्पन को भी काफी देर तक यह समझ नहीं थी कि ये मैंग्रोव पेड़ तूफानों और समुद्री कटाव से तटीय इलाकों की रक्षा कैसे करते हैं। 1990 के दशक के आख़िरी वर्षों में जब वह एक मैंग्रोव जागरूकता कार्यशाला में शामिल हुआ, तब जाकर उसकी सोच में बदलाव आया।
पर्यावरण से जन आंदोलन तक
उस कार्यशाला के बाद वीरप्पन ने गाँवों में लोगों ख़ासकर महिलाओं को संगठित किया। उन्होंने ‘फिशबोन’ नहरें बनाईं, मैंग्रोव के बीज बोए और इन जंगलों का विस्तार किया। उनके अनुमान के अनुसार, 2004 से अब तक उन्होंने खुद 500 से अधिक Rhizophora मैंग्रोव पेड़ लगाए हैं और 25 महिला स्वयं-सहायता समूहों के साथ मिलकर करीब 6,000 पौधे रोपे हैं। वीरप्पन कहते हैं, “एक बार ये पेड़ लग जाएँ, तो अपने आप उगते रहते हैं, किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं।”
सुनामी के बाद आई समझ
2004 की सुनामी के बाद जब मैंग्रोव की भूमिका पर चर्चा बढ़ी, तब वीरप्पन ने कहा, “मेरे लिए यह नया विषय था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने हमें तस्वीरों के ज़रिए बताया कि मैंग्रोव मिट्टी को कैसे कटाव और तूफानों से बचाते हैं। मैं अशिक्षित हूँ, इसलिए उन तस्वीरों ने मुझे गहराई से समझाया। उस दिन मैंने तय किया कि जहाँ भी जगह मिलेगी, वहाँ मैंग्रोव लगाऊँगा।”
समुदाय के साथ परिवर्तन
वीरप्पन का यह संकल्प अकेला नहीं रहा — उन्होंने अपने साथ स्थानीय लोगों को भी जोड़ा। मछुआरे एस. मुरुगन, जो पहले इन पेड़ों को बेकार मानते थे, बताते हैं, “पहले हमें लगता था कि ये बेकार हैं क्योंकि फल नहीं देते। लेकिन वीरप्पन ने हमें समझाया कि ये हमारी ज़मीन और जीवन की रक्षा करते हैं।”
इरुला समुदाय से पर्यावरण योद्धा तक
इरुला समुदाय से आने वाले वीरप्पन की कहानी सिर्फ मैंग्रोव तक सीमित नहीं। सुनामी के बाद उन्होंने CARE India और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के सहयोग से ‘क्रैब फैटनिंग’ (केकड़ों को मोटा करने) की तकनीक सीखी। 2006 में उन्होंने दो महिला समूहों के साथ सात इकाइयाँ बनाई और आज पिचावरम में 10 क्रैब फैटनिंग यूनिट्स चल रही हैं।
वे स्थानीय मछुआरों से छोटे केकड़े खरीदते हैं और उन्हें बैकवॉटर में छोड़ देते हैं ताकि प्रजाति बनी रहे और टिकाऊ मछलीपालन को बढ़ावा मिले।
संरक्षण का नया मॉडल
पिछले 15 वर्षों में वीरप्पन ने 1,000 से अधिक ब्रूडर क्रैब (अंडे देने वाली मादा केकड़े) को बचाया है। जब भी वह किसी को अंडे वाले केकड़े बेचते देखते हैं, तो खुद उन्हें खरीदकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं ताकि उनका प्रजनन हो सके। उनकी बेटी वी. मीरा, जो पिछले दस साल से फैटनिंग यूनिट में काम कर रही हैं, कहती हैं, “अप्पा (पिता) ऐसे केकड़ों को ऊँचे दाम पर भी खरीद लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वे हमेशा कहते हैं — इन्हें बेचोगे तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी।”
पर्यावरण और रोज़गार का संगम
वीरप्पन ने MSSRF के “इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिश फार्मिंग सिस्टम (IMFFS)” में भी हिस्सा लिया है। इसमें उन्होंने 6,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और साथ ही सी-बास मछलियाँ पाली हैं। यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण को आजीविका से जोड़ने की मिसाल बन गया है।
एक आग से मिली सीख
वीरप्पन बताते हैं, “जब मैं 20 साल का था, हमारे घर के पास ज़मीन में आग लगी। कई लोग घायल हुए। दोषियों ने हमें पैसे देने की पेशकश की, पर मेरे पिता ने पूछा — क्या तुम इन जले पेड़ों की जगह नए पेड़ उगा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। तभी मैंने प्रकृति की अहमियत समझी।”
इरुला समुदाय का नया जीवन
इरुला पहले सांप, चूहे आदि का शिकार करके जीवन चलाते थे। लेकिन सख्त वन्यजीव क़ानूनों के बाद उन्हें दूसरे काम अपनाने पड़े। सुनामी के बाद सरकार और एनजीओ ने इस समुदाय को घर और नावें दीं। वीरप्पन, जो कभी स्कूल नहीं गए, अब चार बच्चों के पिता हैं और पर्यावरण योद्धा बन चुके हैं।
महिलाओं को मिला सहारा
क्रैब फैटनिंग यूनिट्स ने गाँव की महिलाओं को आर्थिक मज़बूती दी है। के. शर्मिला, जो 8 साल से इस काम में हैं, बताती हैं, “मैं हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। बारिश के मौसम में जब मछली पकड़ना मुश्किल होता है, तब यही काम सहारा बनता है।”
के. सेल्वी कहती हैं, “मैं जो कमाती हूँ, उसे बेटी की पढ़ाई के लिए बैंक में जमा करती हूँ। भले ही आय कम हो, पर आत्मनिर्भरता का अहसास बड़ा है।”
पुरस्कार और पहचान
MSSRF की कोस्टल रिसोर्सेज प्रमुख एस. वेलविझी कहती हैं, “वीरप्पन ने न केवल पिचावरम के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया, बल्कि इरुला समुदाय की आर्थिक स्थिति भी सुधारी। वे सामुदायिक संरक्षण का जीवंत उदाहरण हैं।”वीरप्पन हाल ही में “डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड 2025” से सम्मानित हुए, जो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने प्रदान किया।
रोटरी क्लब के अध्यक्ष बालाजी श्रीनिवासन ने कहा, “हमने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जो केवल बोलता नहीं, बल्कि बदलाव खुद करता है। वीरप्पन ने दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास एक साथ संभव हैं।”यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बताती है कि जब समुदाय प्रकृति के साथ खड़ा होता है — तो धरती भी बचती है, और इंसान भी।

